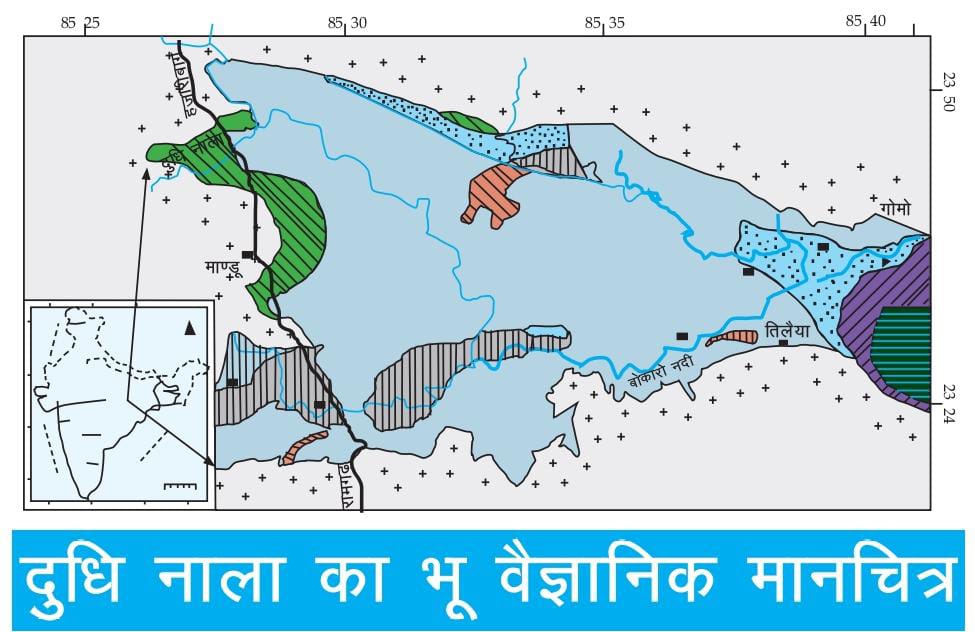(राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस, 24 जुलाई पर विशेष)
योगेश कुमार गोयल
‘थर्मल पावर स्टेशन’ जिन्हें ऊष्मीय शक्ति संयंत्र या ताप विद्युत केन्द्र के नाम से जाना जाता है, ऐसे विद्युत उत्पादन संयंत्र होते हैं, जिनमें प्रमुख टरबाइनें भाप से चलाई जाती हैं। यह भाप कोयला, गैस इत्यादि को जलाकर पानी को गर्म करके प्राप्त की जाती है। पानी गर्म करने के लिए ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जिससे उच्च दबाव पर भाप बनती है और बिजली पैदा करने के लिए इसी भाप से टरबाइनें चलाई जाती हैं। हमारे जीवन में थर्मल इंजीनियरिंग के महत्व को समझाने के लिए प्रतिवर्ष 24 जुलाई को ‘राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस’ मनाया जाता है। यह भी जान लेते हैं कि थर्मल इंजीनियरिंग आखिर है क्या? यह मेकेनिकल इंजीनियरिंग का ही एक ऐसा हिस्सा है, जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। घरों तथा गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले एयरकंडीशनर तथा रेफ्रिजरेटरों में इसी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है। थर्मल इंजीनियरिंग के जरिये इंजीनियर ऊष्मा को अलग-अलग माध्यमों में उपयोग करने के अलावा ऊष्मीय ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में भी परिवर्तित कर सकते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग बंद या खुले वातावरण में वस्तुओं को गर्म या ठंडा रखने की प्रक्रिया है। थर्मल इंजीनियर ऊष्मीय ऊर्जा को केमिकल, मेकेनिकल या विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें तैयार करते हैं, जिनके जरिये वे ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं। हमारे घरों या दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली इसी ऊष्मीय ऊर्जा से बनती है। यह बिजली बनाने का काम करते हैं थर्मल पावर स्टेशन।थर्मल पावर स्टेशनों में ऊष्मीय ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए भाप से चलने वाली टरबाइनों का इस्तेमाल किया जाता है। भाप बनाने के लिए पानी को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इसके लिए कोयला, सोलर हीट, न्यूक्लियर हीट, कचरा तथा बायो ईंधन उपयोग किया जाता है। दुनिया के कई देशों में अभी भी बिजली पैदा करने के लिए भाप से चलने वाली टरबाइनों का उपयोग किया जाता है किन्तु पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए अब धीरे-धीरे बिजली पैदा करने के लिए सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोतों को ही महत्व दिया जाने लगा है। दरअसल, थर्मल पावर स्टेशनों में भाप पैदा करने के लिए कोयला जलाने से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचती है। इस प्रक्रिया में निकलने वाली हानिकारक गैसें हवा में मिलकर पर्यावरण को बुरी तरह प्रदूषित करती हैं। साथ ही कोयला या अपशिष्ट जलाने के बाद बचने वाले अवशेषों के निबटारे की भी बड़ी चुनौती रहती है। हालांकि भारत में थर्मल पावर स्टेशनों में बिजली पैदा करने के लिए कोयले के अलावा ऊर्जा के अन्य स्रोतों का भी इस्तेमाल किया जाता है किन्तु अधिकांश बिजली कोयले के इस्तेमाल से ही पैदा होती है। विश्वभर में करीब 40 फीसदी बिजली कोयले से ही प्राप्त होती है जबकि देश में करीब 60 फीसदी बिजली कोयले से, 16.1 फीसदी अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा बायो गैस से, 14 फीसदी पानी से, 8 फीसदी गैस से, 1.8 फीसदी न्यूक्लियर ऊर्जा से तथा 0.3 फीसदी डीजल से पैदा होती है। यह जान लेना भी जरूरी है कि बिजली पैदा करने के लिए भले ही ऊर्जा के किसी भी स्रोत का इस्तेमाल किया जाए, हरेक थर्मल पावर प्लांट में इसके लिए बॉयलर का इस्तेमाल होता ही है। जिसमें ईंधन को जलाकर ऊष्मीय ऊर्जा पैदा की जाती है। पानी को गर्म कर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइनों को चलाने में इस्तेमाल होती है।आज दुनियाभर में वायु प्रदूषण एक बड़े स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर रहा है। इस समस्या के लिए थर्मल पावर प्लांटों से निकलने वाला उत्सर्जन भी एक बड़ा कारण है। इस समस्या से निपटने के लिए एक दशक से भी अधिक समय से उत्सर्जन मानकों को पूरा करने और नए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को रोककर अक्षय ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इन उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करता रहा है किन्तु थर्मल पावर प्लांट के लिए उत्सर्जन मानकों को लागू करने का मामला वर्षों से अधर में लटका है। पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए अब पर्यावरण पर कार्य कर रही कुछ संस्थाओं द्वारा मांग की जाने लगी है कि पर्यावरण मंत्रालय उत्सर्जन मानकों का पालन करने की जिम्मेदारी का वहन करते हुए थर्मल पावर प्लांटों को प्रदूषण के लिए उत्तरदायी बनाए और अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए थर्मल पावर प्लांटों का निर्माण रोका जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोयले को जलाया जाना और इससे होने वाली गर्मी, पारे के प्रदूषण का मुख्य कारण है। माना जा रहा है कि उत्सर्जन मानकों का पालन करने में देरी के चलते सालभर में 70 हजार से भी अधिक समय पूर्व मौतें हो रही हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत संस्था ग्रीनपीस के अनुसार अगर उत्सर्जन मानकों को समय से लागू किया जाता तो सल्फर डाई ऑक्साइड में 48 फीसदी, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड में 48 फीसदी और पीएम उत्सर्जन में 40 फीसदी तक की कमी की जा सकती थी। जिससे समय पूर्व हो रही इन मौतों से बचा जा सकता था। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टि से पश्चिमी देशों में अब चरणबद्ध तरीके से कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। आईसलैंड तो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन चुका है, जहां अक्षय ऊर्जा से ही सौ फीसदी बिजली पैदा की जा रही है। इसके अलावा स्वीडन, जर्मनी, यूके, कोस्टारिका, निकरागुआ, उरूग्वे इत्यादि देश भी आगामी दो वर्षों के भीतर अक्षय ऊर्जा से ही सौ फीसदी बिजली उत्पादन के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन भी कोयले से बिजली बनाने वाले अधिकांश बिजली संयंत्रों को बंद करने का फैसला कर चुकी है। अमेरिका भी कोयला प्लांट्स को बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन में हालांकि ऐसे गिने-चुने ही पावर प्लांट बचे हैं और उन्हें भी 2025 तक बंद कर दिए जाने की उम्मीद है।कोयले से बिजली उत्पादन करने वाले थर्मल पावर प्लांट इसलिए खतरनाक माने जा रहे हैं क्योंकि कोयले से बिजली बनाने की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा पारे के अलावा बड़ी मात्रा में राख भी निकलती है। ये सभी तत्व पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद खतरनाक माने जाते हैं। वातावरण में इन विषैले तत्वों या गैसों की मात्रा बढ़ने से अनेक गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं। ऐसे पावर प्लांटों के आसपास 100 किलोमीटर से भी अधिक के दायरे में प्रदूषण की मार लोगों पर देखने को मिली है। करीब 300 किलोमीटर क्षेत्र में लिए गए वनस्पतियों और मिट्टी के नूमनों में भी पारे प्रदूषण की उपस्थिति पाई गई है। ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के नाखूनों और बालों में भी पारा मिला है। एक सर्वे में ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों में अनिद्रा, थकान, कमजोरी, याददाश्त की कमी, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, कंपकंपी इत्यादि लक्षण भी देखे गए हैं। इन क्षेत्रों के भूजल के स्रोतों में फ्लोराइड के साथ पारा मिल जाने से ‘फ्लूरोसिस’ जैसी बीमारी भी पनप रही है। थर्मल पावर प्लांटों में बिजली बनाए जाने के लिए कोयला जलाने के दौरान उससे बनी राख का 10 फीसदी से भी अधिक हिस्सा चिमनियों के जरिये धुएं के साथ ही वातावरण में घुल जाता है, जो गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनता है। बहरहाल, समय के साथ अब जरूरत इसी बात की है कि दूसरे देशों की भांति हम भी अक्षय ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाएं और बिजली बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से ऊर्जा के इन्हीं सुरक्षित स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा दें।
This post has already been read 15244 times!